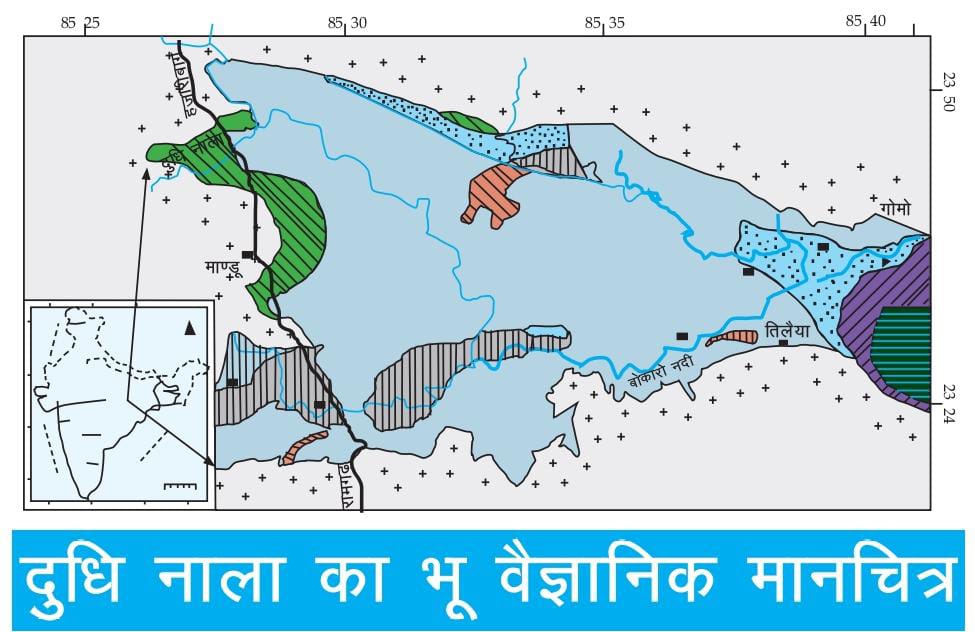मोनिका आर्या
पिछले चार साल में स्पेशल एडॉप्शन एजेंसीज यानी शिशु गृहों में रह रहे करीब 1300 बच्चे (1265) मौत का शिकार हो गए। इनमें अधिकांश वे शिशु शामिल थे, जो एबेंडन यानी परित्यक्त अवस्था में मिले थे। ये किसी अखबार या संस्था का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये सरकार का जवाब है, जो कांग्रेस नेता शशि थरूर के सवाल पर संसद में दिया गया है। सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार ने थरूर के लिखित सवाल के जवाब में यह आंकड़ा सदन के सामने रखा। इस आंकड़े के मुताबिक, बच्चों की सबसे अधिक 292 मौत 2017 से 2018 के दौरान हुईं। यही नहीं, इस आंकड़े पर विश्वास करें (अविश्वास का कोई कारण नहीं) तो महाराष्ट्र में स्थिति सबसे भयावह है, जहां इस दौरान शिशु गृहों में रह रहे 172 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए। हालांकि सरकार ने इन बच्चों की मौत के कारणों का जिक्र नहीं किया है, और न ही उनकी उम्र इसमें बताई गई है। यह आंकड़ा और इससे संबंधित रिपोर्ट एक अंग्रेजी दैनिक में छपी है। सरकार की ओर से अन्य भी कई जानकारियां रखी गई हैं, जिनमें देशभर में सरकार से संबद्ध शिशु गृहों की संख्या, इनमें रह रहे बच्चों की संख्या आदि शामिल है। तथ्यों के लिहाज से आंकड़ें चौंकाने वाले हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि सरकार के पास मौजूद ये आंकड़े भी अधूरे हैं। अखबार में कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसॉर्स अथॉरिटी के सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि जिन बच्चों की मौत हुई, उनमें अधिकांश वे शामिल हैं, जो परित्यक्त या कहें कि एबेंडन स्थिति में मिलते हैं। ये जिन हालात में मिलते हैं, उनमें इनके बचने की उम्मीद कई बार नहीं के बराबर होती है। कारा राष्ट्रीय स्तर पर इकलौती एजेंसी है, जो वैध एडॉप्शन करवाती है और इसलिए इन शिशु गृहों के सीधे संपर्क में होती है। क्योंकि श्री थरूर ने 2014 से पहले का आंकड़ा नहीं मांगा, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इन शिशु गृहों में बच्चों की स्थिति पहले कैसी थी। किसी भी स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन तभी संभव है, जब उससे संबंधित सभी तथ्य सामने हों। इस आंकड़ा, रिपोर्ट और सवाल-जवाब का जिक्र करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति या पार्टी विशेष पर कोई सवालिया निशान लगाना नहीं, अपितु उस मुद्दे को उठाना है, जो अभी भी कई परतों के नीचे छुपा है, और जिस पर अभी भी मनों पक्की धूल जमी है- शिशु परित्याग यानी उनकी हत्या का प्रयास और उनकी हत्या। कारा के सूत्रों ने जो कहा, वह सही बात है। ये अबोध बच्चे जिन हालातों में मिलते हैं, उनकी कल्पना भी दुरूह है। उसे इन बच्चों की हत्या के प्रयास के रूप में ही दर्ज करने की जरूरत है। ये चींटियों और कीड़ों द्वारा और कई बार आवारा जानवरों द्वारा भी खाए हुए मिलते हैं। इनमें इन्फेक्शन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो ऊपर से देखने से नजर नहीं आता। बाहरी और आंतरिक प्राणघातक चोट लगी होती है और मौसम का असर भी इनके लिए जानलेवा साबित होता है। कितने ही बच्चे वहीं दम तोड़ देते हैं, जहां उन्हें छोड़ा या त्यागा गया होता है। कई बार छोड़ा ही इस तरह जाता है कि उनके जीवित बचने की कोई उम्मीद न बचे। जो बचते हैं, वे ही शिशु गृहों तक पहुंच पाते हैं, और उनमें से भी कितने इलाज के दौरान काल के गाल में समा जाते हैं। इतना ज्वलंत मुद्दा होने के बावजूद आज तक यह किसी की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं हो पाया। किसी व्यक्ति, संस्था या पार्टी ने कभी इसे किसी सार्वजनिक या सामाजिक मंच पर नहीं उठाया। कोई नहीं जानता कि सड़कों, कूड़े के ढेरों, झाड़ियों, नालियों में कितने नवजात शिशु मार दिए जाते हैं, जिन्हें बाद में स्टिलबर्थ का केस या भ्रूण हत्या समझ कर भुला दिया जाता है। कितने ही राज्यों में इन बच्चों की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। इसलिए इनकी सही संख्या भी पता नहीं चलती। इस मामले में हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी और राजस्थान से लेकर मेघालय तक एक जैसी लापरवाही नजर आती है। संस्था सरकारी हो या गैर सरकारी, महज शिशु गृहों की मार्फत इन नवजातों का जीवन संवारने का सपना संजोये हैं, लेकिन ये सोचने की ज़हमत कोई नहीं उठा रहा कि बच्चे बचेंगे ही नहीं, तो शिशु गृह पहुंचेंगे कैसे और वे उनका जीवन संवारेंगे कैसे। राज्यों की राजधानियों में सरकारी सहयोग से बच्चों से जुड़े तमाम मुद्दों- बाल विवाह, कन्या शिक्षा, भ्रूण हत्या, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर आदि पर बड़े बड़े कार्यक्रम, वर्कशॉप्स, सेमीनार, ओरियंटेशन आयोजित होते हैं। इनसे अलग कभी शिशु परित्याग या उनकी हत्या पर कोई कार्यक्रम कहीं हुआ हो, ऐसा नजर से नहीं गुजरा। यहां तक कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश भी इस दिशा में निराश करते हैं, जहां शिशु परित्याग और उनकी हत्या चरम पर हैं।
आमतौर पर एनसीआरबी का आंकड़ा देखकर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि को इन बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों की संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन उन राज्यों का क्या, जहां इन घटनाओं पर व्यवस्था द्वारा चुप्पी की चादर ओढ़ ली जाती है। ये घटनाएं बहुतायत में होती हैं, लेकिन महज यूडी में दर्ज होकर रह जाती हैं, इसलिए किसी डेटा में इनका कोई जिक्र नहीं होता। क्या हालात उन राज्यों में ज्यादा खराब नहीं हैं, जहां एनसीआरबी का डेटा जीरो बताता है। बड़ी चिंता इस बात की है कि ये बच्चे त्यागने से पहले ही सहेज लिए जाएं, इसके लिए कोई सार्थक और उपयोगी कदम नहीं उठाया जा रहा। इस मुद्दे पर सिस्टम खुद इतना अनजान है कि वह जानकारी दुरूस्त करने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में भी नहीं सोच पाता। लोगों को प्रभावी तरीके से बता नहीं पाता कि उन्हें क्या करना है। आमजन को बताने से पहले सिस्टम को खुद ये जानना होगा कि सड़कों पर मृत मिल रहे बच्चों के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है। बच्चों के संरक्षण के लिए बनाए गए इतने बड़े बेड़े में किसकी जिम्मेदारी है उन मृत बच्चों का संज्ञान लेने की और उन्हें मौत से बचाने की। नवजातों के जीवन में लगते इस ग्रहण के लिए ज्यादा दोष उन एजेंसियों का नजर आता है, जिन्हें इन बच्चों के संरक्षण का जिम्मा सौंप सरकार निश्चिंत हो जाना चाहती है। समाज में हो रही गतिविधि से इन एजेंसियों का प्रत्यक्ष साबका पड़ता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज, जिला बाल संरक्षण ईकाइयां, बाल संरक्षण आयोग जैसी सरकारी एजेंसियां यदि चाहें, तो अन्य मुद्दों की भांति शिशु परित्याग और उनकी हत्या जैसे अपराध पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सिस्टम और समाज में जागरूकता का जो अकाल है, उसकी भरपाई कर सकती हैं, लेकिन वहां फंड की बंदरबांट और उसमें मिलने वाले कमीशन को लेकर हायतौबा मची रहती है। उनका ध्यान कभी इस तरफ जाता ही नहीं। बची खुची राशि के सहारे सरकारी प्रयासों का दिखावा तो हो सकता है, वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं। यूं भी उनकी चेष्टा कभी बड़ी लकीर खींचने की नहीं होती।
This post has already been read 85714 times!