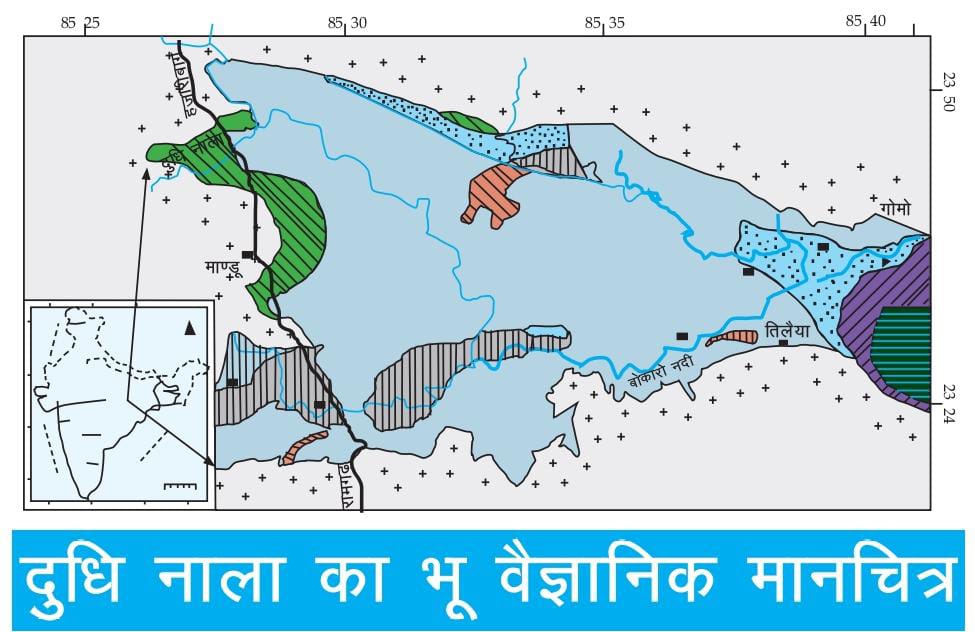-योगेश कुमार गोयल-
दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहर प्रदूषण के चलते बुरी तरह हांफ रहे हैं। पिछले कुछ समय से देश में पर्यावरण का मिजाज लगातार बिगड़ रहा है। इसका खामियाजा देश ने वर्षभर किसी न किसी बड़ी आपदा के रूप में भुगता है। पर्यावरण संबंधी कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में स्पष्ट हो चुका है कि भारत के कई शहर दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु प्रदूषण डाटाबेस के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 15 शहरों में से 14 भारत में हैं। इनमें वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, पटना तथा गया शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली की हालत तो अक्सर गैस चैंबर सरीखी होती रही है, जहां जब-तब जहरीली धुंध का गुबार देखने को मिलता है। इससे किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मेडिकल जर्नल ‘द लांसेट’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण के चलते प्रतिवर्ष दस लाख से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कार्बन उत्सर्जन मामले में दिल्ली दुनिया के 30 शीर्ष शहरों में शामिल है। यहां पहाड़नुमा कूड़े के ढेरों से निकलती जहरीली गैसें, औद्योगिक इकाईयों से निकलते जहरीले धुएं के अलावा सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या कार्बन उत्सर्जन का बड़ा कारण है। कहा जाता है कि अगर दिल्ली तथा देश के अन्य अत्यधिक प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है तो लोगों को निजी वाहनों का प्रयोग कम कर सार्वजनिक परिवहन को अपनाना चाहिए। साथ ही बड़े पैमाने पर पौधारोपण को बढ़ावा देकर हरियाली बढ़ानी होगी। लेकिन वास्तव में देश में पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हो क्या रहा है? पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े-बड़े दावे और वादों के बावजूद वृक्षों के विनाश का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। हरियाली की कमी के चलते पर्यावरण का संतुलन डगमगाने से प्रकृति का प्रकोप बार-बार सामने आ रहा है। दूसरी ओर, सरकारें ही शहरी विकास, देश के विकास को रफ्तार देने या लंबे-चौड़े एक्सप्रेस-वे बनाने के नाम पर लाखों वृक्षों का सर्वनाश करने का फरमान जारी करने में विलम्ब नहीं करतीं। कुछ माह पहले दिल्ली में 16500 ऐसे ही पेड़ काटे जाने का फरमान सुनाया गया था, किन्तु ‘चिपको आन्दोलन’ की तर्ज पर दिल्लीवासियों ने व्यापक स्तर पर जन अभियान चलाकर दिल्ली सरकार को अपना निर्णय वापस लेने को विवश कर इन वृक्षों को कटने से बचा लिया। लेकिन देश में हर जगह स्थिति ऐसी नहीं है। हिमालयी क्षेत्र हो या गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र, हर जगह हजारों की संख्या में विशालकाय वृक्ष बेरहमी से काटे जा रहे हैं। चारधाम यात्रा को सुखद बनाने के लिए सड़कों के चौड़ीकरण के लिए करीब नौ सौ किलोमीटर के दायरे में वर्षों पुराने लाखों हरे-भरे वृक्ष काट डाले गए। माना कि देश के विकास को रफ्तार देने के लिए चौड़े एक्सप्रेस-वे बनाना समय की मांग है किन्तु सरकारी मशीनरी इस बात का जवाब कब देगी कि विकास के नाम पर बेरहमी से देशभर में लाखों वृक्षों के विनाश के चलते पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में हरे-भरे वृक्षों के विनाश के चलते मानव सहित समस्त प्राणी जगत का जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? जीवन ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो यह विकास किस काम का? हम क्यों नहीं समझना चाहते कि जैसे-जैसे सघन वनों का दायरा घटेगा, देश में बाढ़, सूखा, स्मॉग जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दायरा बढ़ता जाएगा। वृक्ष न केवल हमें भावनात्मक तथा आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं बल्कि मिट्टी को रोके रखकर हमें बाढ़ के खतरे से बचाते हैं। कार्बन डाईऑक्साइड को अवशोषित कर आसपास के वायुमंडल को स्वच्छ रखते हैं। वर्षा कराने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विषैले पदार्थों को अवशोषित करते हुए पोषक तत्वों का नवीनीकरण करते हैं। खाद्य सामग्री तथा औषधियां उपलब्ध कराते हैं। उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं तथा वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। यदि विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण करना ही है तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं तलाशा जाना चाहिए, जिससे अधिकांश वृक्षों को बचाते हुए विकास कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। न्यूयार्क के पर्यावरण संरक्षण विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 विशाल वृक्ष प्रतिवर्ष 53 टन कार्बन डाईऑक्साइड तथा 200 किलोग्राम अन्य वायु प्रदूषकों को दूर करते हैं और पांच लाख तीस हजार लीटर वर्षा जल को थामने में भी मददगार साबित होते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार घर में सुनियोजित ढंग से लगाए जाने वाले वृक्ष न केवल गर्मियों में एसी की खपत में 56 फीसदी की कमी लाते हैं बल्कि सर्दियों में ठंडी हवाओं को भी रोकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वृक्षों से भरे परिवेश में रहने वाले व्यक्ति ज्यादा सुरक्षित तथा मिलनसार स्वभाव के होते हैं। एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि किसी भी वृक्ष के वजन में एक ग्राम की वृद्धि से ही उससे 2.66 ग्राम अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है। भारतीय वन सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सघन वनों का क्षेत्रफल तेजी से घट रहा है। 1999 में सघन वन 11.48 फीसदी थे, जो 2015 में घटकर मात्र 2.61 फीसदी ही रह गए। रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई राज्यों उत्तराखण्ड, मिजोरम, तेलंगाना, नगालैंड, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, झारखण्ड, दादर नागर हवेली इत्यादि में वन क्षेत्र तेजी से कम हुए हैं। सघन वनों का दायरा सिमटते जाने के चलते ही वन्यजीव शहरों-कस्बों का रूख करने पर विवश होने लगे हैं। ‘नेचर’ जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस समय करीब 35 अरब वृक्ष हैं। इस लिहाज से प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में करीब 28 वृक्ष आते हैं। यह आंकड़ा पढ़ने और सुनने में जितना सुखद प्रतीत होता है, उतना है नहीं। क्योंकि, इन 35 अरब वृक्षों में से अधिकांश सघन वनों में हैं, न कि देश के विभिन्न शहरों या कस्बों में। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के चलते सघन वनों का क्षेत्रफल भी तेजी से घट रहा है। किसी भी क्षेत्र में वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए वहां वन क्षेत्र 33 फीसदी होना चाहिए किन्तु दिल्ली में यह सिर्फ 11.88 फीसदी है। दिल्ली से सटे इलाकों फरीदाबाद, नोएडा तथा गाजियाबाद में यह क्रमशः 4.32, 2.43 तथा 1.89 फीसदी ही है। कैग की एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो दिल्ली पहले से ही करीब नौ लाख वृक्षों की कमी से जूझ रही है। पिछले पांच वर्षों में हरियाली घटने से दिल्ली में वायु प्रदूषण करीब चार सौ फीसदी बढ़ा है। देश में मौसम चक्र जिस तेजी से बदल रहा है, जलवायु संकट गहरा रहा है, ऐसी पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने का एक ही उपाय है वृक्षों की सघनता। वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण अथवा भू-क्षरण, इन समस्याओं से केवल ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर ही निपटा जा सकता है। स्वच्छ प्राणवायु के अभाव में लोग तरह-तरह की भयानक बीमारियों के जाल में फंस रहे हैं। उनकी प्रजनन क्षमता पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उनकी कार्यक्षमता भी इससे प्रभावित हो रही है। कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का संक्रमण, न्यूमोनिया, लकवा इत्यादि के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा इन बीमारियों के इलाज पर ही खर्च हो जाता है। हम प्रकृति से अपने हिस्से का ऑक्सीजन तो ले लेते हैं किन्तु प्रकृति को उसके बदले में लौटाते कुछ भी नहीं। एक सामान्य वृक्ष सालभर में लगभग सौ किलो ऑक्सीजन देता है जबकि एक व्यक्ति को वर्षभर में साढ़े सात सौ किलो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नीम, बरगद, पीपल जैसे बड़े छायादार वृक्ष, जो 50 साल या उससे ज्यादा पुराने हों, उनसे तो प्रतिदिन 140 किलो तक ऑक्सीजन मिलती है। इस हिसाब से अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि ऐसे छायादार पुराने वृक्ष काटने से पर्यावरण को कितनी क्षति पहुंचती है। यही वजह है कि ऐसे छायादार वृक्ष अपने आसपास के परिवेश में लगाने की प्राचीन भारतीय परम्परा रही है। हमें यह बात भली-भांति समझ लेनी चाहिए कि यदि वृक्ष बचे रहेंगे, तभी पृथ्वी पर जीवन बचेगा।
This post has already been read 24920 times!