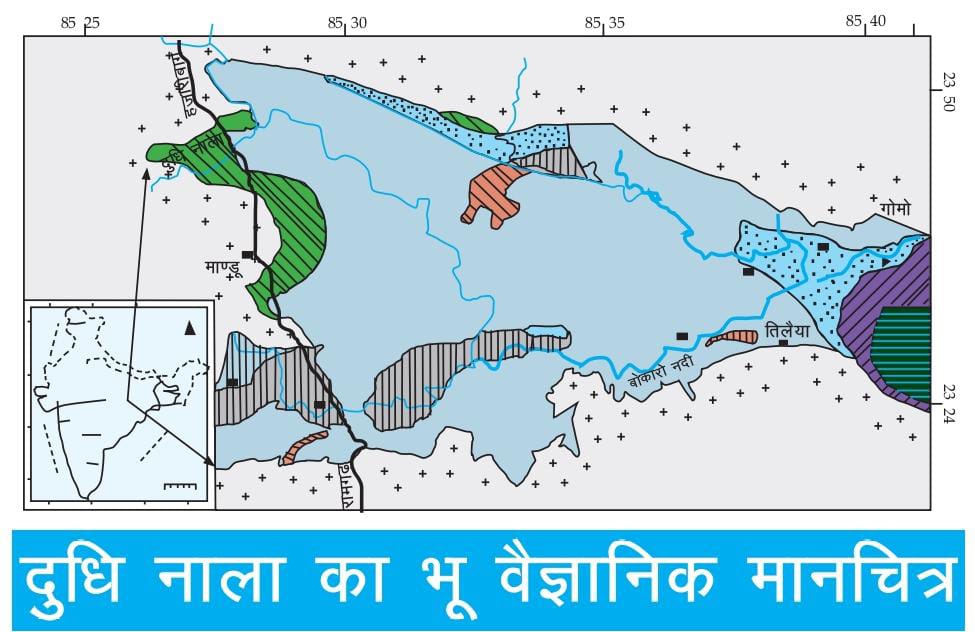डॉ. राकेश राणा
‘सूचना’ या संचार क्रांति उत्तर आधुनिक युग की मुख्य पूंजी है। समाज-वैज्ञानिक समाज को सूचना समाज अथवा ज्ञानमूलक-समाज जैसे मुहावरों से नवाज रहे हैं। संचार क्रांति ने आधुनिक समाज और व्यक्ति के विकास में महती भूमिका निभाई है। संचार क्रांति ही समाज में सामाजिक चेतना का आधार है। मनुष्य विभिन्न सूचनाओं को संयोजित कर तार्किक पद्धति द्वारा ज्ञान में तब्दील करता है। जिसके आधार पर अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर भावी संकल्पनाएं गढ़ता है। इससे मनुष्य में दृष्टिकोण और पर्यवेक्षण क्षमता विकसित होती है। धीरे-धीरे यह प्रतीकात्मक व्यवस्था अपने समाज के सदस्यों के हित के लिए एक बौद्धिक समुदाय का गठन कर लेती है। आधुनिक ‘सूचना-तंत्र’ ने समाज की इस विकास प्रक्रिया को तीव्र और मजबूत किया है। यह संचार माध्यमों से ही संभव हो पाया है। दुनिया विश्व ग्राम बन गयी है। आज विश्व-ग्राम की छह अरब से अधिक जनसंख्या की सूचना सहक्रिया, ज्ञान और बुद्धि के आधार पर ही समाज का विकास विश्व स्तर पर संभव हो पाया है। टी.वी., कंप्यूटर, इन्टरनेट, मल्टीमीडिया, वर्चुअल रीयलिटी, डिजिटल, वीडियो, ऑडियो, थ्री.डी. ग्राफिक्स जैसे सूचना संवाहक विश्व समाज को ‘ज्ञान मूलक’ समाज के रूप में निरूपित कर रहे हैं। घर बैठे दुनिया के किसी कोने में वीडियो कान्फ्रेंस कर सकते हैं। किसी अकादमिक बहस में शरीक हो सकते हैं, सुन सकते हैं। घर बैठे चैबीसों घंटे ऑफिस चला सकते हैं। ड्राइंग रूम में बैठे-बैठे टेलीशॉपिंग कर चाहे जो मंगा सकते हैं। दुनिया की कोई भी जानकारी जब चाहे तब ले सकते हैं। यह आधुनिक संचार तंत्र की महत्वपूर्ण देन है। शहरों से कटे दूर-दराज के अंचलों के लोग इन माध्यमों से रूबरू हो रहे हैं। सात-समन्दर पार नौकरी करने वालों से जब बुढ़िया दादी टेलीफोन और मोबाइल पर बात कर खुश होती है तो दुनिया वाकई गांव नजर आती है। इसका श्रेय संचार क्रांति को जाता है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में मॉस मीडिया की भूमिका की महत्ता और व्यापकता को इसी से समझा जा सकता है कि सदियों से जिस भारतीय समाज को ‘मौखिम समाज’ के रूप में जाना गया, वैश्वीकरण के दौर में उसे ‘मीडिया समाज’ के रूप में देखा जा रहा है।आज देश में लगभग 700 चैनल हैं। भारत में ज्यादातर चैनल चौबीस घंटों वाले हैं। विश्व स्तर पर हुआ एक अध्ययन बताता है कि भारत में टी.वी. प्रसार की दर अन्तराष्ट्रीय प्रसार दर से अधिक है और भारत में यह दर निरन्तर बढ़ रही है। चैनलों की बाढ़ आ रही है। सात हजार के आसपास अखबार व पोर्टल सूचना विनिमय में संलग्न हैं। ग्लोबल-मीडिया के आधुनिक संचार माध्यमों के परिणाम स्वरुप तीसरी दुनिया के विकासशील समाजों में जिस तरह के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन घटित हो रहे हैं। एक विशाल उपभोक्ता वर्ग खड़ा हो रहा है, वह इन मीडिया विस्फोटों का ही परिणाम है। वैश्विक मीडिया द्वारा विकासशील समाज में जिस तरह के दबाव बनाये जा रहे हैं, उससे इन समाजों की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनायें ही खतरे में पड़ गईं। विकासशील गरीब देश उसका सबसे आसान शिकार हैं। यूरोपीय देश तक इससे भयभीत हैं। फ्रांस जैसा मजबूत सांस्कृतिक आधार वाला देश अपनी अस्मिता को लेकर चिंतित है। ब्रिटेन सहमा हुआ है। फिर इस गरीब तीसरी दुनिया की तो बिसात ही क्या है। इन समाजों के सम्मुख अहम् चुनौती यह है कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और बाजारवाद से लड़ाई कैसे लड़ी जाए या आत्मसमर्पण कर दिया जाए? क्योंकि आज सूचना तंत्रों पर बडे़-बड़े निगमों, घरानों, पूंजीपतियों का नियंत्रण नहीं है। आधुनिक पूंजीवादी वैश्विक समाज को आर्थिक सांस्कृतिक ढांचे की बुनियादी इकाई बहुराष्ट्रीय निगम है। विश्व बाजार पर अपना आधिपत्य और नियंत्रण कायम रखने के लिए ग्लोबल मीडिया का उपयोग करते हैं। सूचना और सांस्कृतिक वर्चस्व के द्वारा यह कार्य आसान हो जाता है। संचार माध्यमों के विशेषज्ञ अमेरिकी हरबर्ट आर्ह शिलर कहते हैं कि इन क्षेत्रों पर प्रभुत्व कायम करना अल्पकालिक जरूरत नहीं बल्कि स्थायी शर्त है जो बाजार व्यवस्था तथा उसके विधि विधानों के गर्भ से पैदा होती है। संचार प्रोद्यौगिकी की छत्रछाया में वैश्वीकरण के दौर में दुनिया जिस तेजी से समरूपता की तरफ बढ़ रही है, वह समाज वैज्ञानिकों की चिंता का गंभीर विषय है। क्या यह सूचना क्रांति समाजों की पहचान, कला, कौशल और हुनर को खतरा पैदा कर सकती है? या उन्हें और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करेगी? आधुनिक वैश्विक दुनिया के सम्मुख यह एक बड़ा सवाल है। पिछले दशकों में मीडिया ने विकासशील समाजों में जिस मानसिकता को रोपा है अब वह धीरे-धीरे एक रूप लेने लगी है। उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार रातोंरात नहीं हो गया है। यह मीडिया द्वारा बड़े सुनियोजित ढंग से हमारे दिमागों में रचाया-बसाया गया है। युवाओं के मध्य जो ग्लोबल-कल्चर विकसित हुई है उसका श्रेय इसी मीडिया को ही जाता है। क्योंकि, वह जोर-शोर के साथ किशोरों और यवुाओं को समर्पित है। इसमें बुजुर्गों का दखल कहीं है ही नहीं। साथ ही साथ आधुनिक पूंजीवादी मूल्यों का इसे पूरा समर्थन है। जो इस दौर के मुख्य तर्क बाजार को ज्यादा प्रमुखता देते हैं। इस पूरे वातावरण के साथ जो संस्कृति विकसित हो रही है उसमें पाप-पुण्य, सही-गलत, धर्म-अधर्म, नैतिक-अनैतिक, शुभ-अशुभ के द्वन्द्व कहीं है ही नहीं। यह नीति निरपेक्ष संस्कृति ही आज की ग्लोबल-कल्चर है जिसे पापुलर कल्चर या वैश्विक संस्कृति कहा जा रहा है। जो संचार क्रांति पर सवार होकर पूरे विश्व की परिक्रमा करती घूम रही है। इसके सहारे बनने वाला विश्व-ग्राम उस शॉपिंग काम्पेक्स की तरह है जहां सब उत्पाद, एक साथ और एक ही तरह से देखे और भोगे जा रहे हैं। मैकडोनाल्ड के बर्गर-न्यूयार्क से दिल्ली तक, मुंबई से बनारस तक, एक ही ढंग से निर्मित रेस्टोरेन्ट, एक ही पैटर्न के सेल काउन्टर और एक ही स्वाद के साथ लोगों तक पहुंचाये जा रहे हैं। संचार क्रांति से निर्मित इस वैश्विक दुनिया में जितना ग्लोबल लोकल हुआ है उतना ही लोकल ग्लोबल भी हुआ है। आज विकासशील समाजों में विकसित समाजों की झलक दिखाई पड़ती है। यह अच्छा भी लगता है और खतरनाक भी। क्योंकि, समरुपता उस वैविध्य के सौन्दर्य को निगल जाएगी जो इन परम्परागत समाजों का वास्तविक सौन्दर्य भी था और पहचान भी। फिर भी सूचना या संचार क्रांति आज की बड़ी ताकत है।
This post has already been read 13657 times!